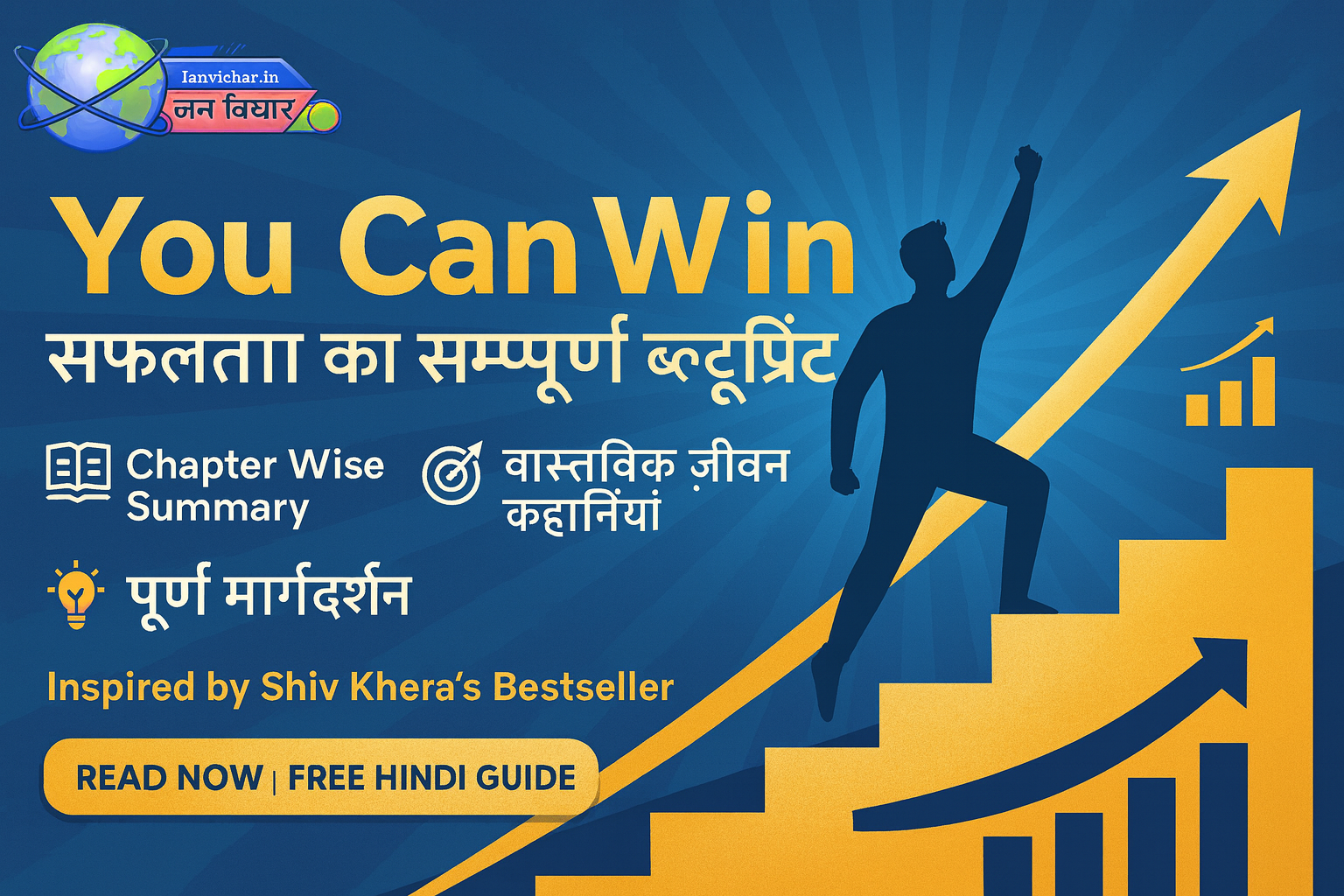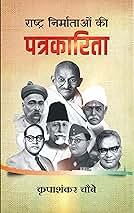
प्रो. कृपाशंकर चौबे जी देश के वरिष्ठ एवं सम्मानित पत्रकार , साहित्यिक व ऐतिहासिक विशेषज्ञ एवं विभागाध्यक्ष जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। प्रो. चौबे अनेकों प्रतिष्ठित अखबार में संपादक रहें हैं। प्रो. कृपाशंकर चौबे द्वारा अनेकों विषय संबंधित अनेकों किताबें भी लिखित हैं। प्रो. चौबे द्वारा गांधी एवं गांधी की पत्रकारिता पर विस्तृत जानकारी लिखी गई है।
निबंध
महात्मा गांधी की पत्रकारिता
कृपाशंकर चौबे
महात्मा गांधी के पत्रकारीय लेखन की शुरुआत लंदन से जोसिया ओल्डफील्ड के संपादन में छपनेवाली साप्ताहिक पत्रिका ‘द वेजेटेरियन’ से हुई थी। उस पत्रिका के 07-02-1891 के अंक में ‘भारतीय अन्नाहारी’ शीर्षक गांधीजी के लेख की पहली किस्त छपी जिसमें उन्होंने कहा था, “भारत में ढाई करोड़ लोग निवास करते हैं। वे भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के हैं। व्यवहार में प्रायः सभी भारतीय अन्नाहारी अथवा निरामिषाहारी हैं।” ‘द वेजेटेरियन’ के 14-02-1891 के अंक में ‘भारतीय अन्नाहारी’ की दूसरी, 21-02-1891 को तीसरी, 28-02-1891 को चौथी, 07-03-1891 को पांचवीं और 14 मार्च 1891 को ‘भारतीय अन्नाहारी’ की छठी किस्त छपी। गांधी जी ने ‘कुछ भारतीय त्यौहार’ शीर्षक लेख ‘द वेजेटेरियन’ के 28-03-1891, 04-04-1891, 25-04-1891 के अंकों में तीन किस्तों में लिखा। गांधीजी ने ‘वेजटेरियन मेसेंजर’ के एक जून 1891 के अंक में ‘भारत के आहार’ शीर्षक लंबा लेख भी लिखा। ‘वेजेटेरियन’ में छपे गांधीजी के लेख संपूर्ण गांधी वाडमय के प्रथम खंड में संकलित हैं। वे पत्रकारीय लेख तब लिखे गए थे जब गांधीजी लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधीजी 1891 में भारत लौटे। 1893 में एक कानूनी काम मिलने पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां जाते ही उन्हें रंगभेद के एक नहीं, अनेक अनुभव हुए। उन्होंने वहां रहकर जातीय पूर्वाग्रहों के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतवंशियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गांधीजी ने 04 जून 1903 को साप्ताहिक समाचार पत्र ‘इंडियन ओपिनियन’ निकाला। मदनजीत व्यावहारिक नामक एक गुजराती सज्जन के प्रेस से वह छपा। गांधीजी ने अपनी पुस्तक ‘दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास’ में लिखा है, “दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी प्रेस खोलने का श्रेय श्री मदनजीत व्यावहारिक नामक एक गुजराती सज्जन को है।”1’सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा’ पुस्तक में भी गांधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ का विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है, “श्री मदनजीत ने ‘इंडियन ओपिनियन’ अखबार निकालने का विचार किया। उन्होंने मेरी सलाह और सहायता मांगी। छापाखाना तो वे चला ही रहे थे। अखबार निकालने के विचार से मैं सहमत हुआ। सन् 1904 में इस अखबार का जन्म हुआ। मनसुखलाल नाजर इसके संपादक बने। पर संपादन का सच्चा बोझ तो मुझ पर ही पड़ा। मेरे भाग्य में प्रायः हमेशा दूर से ही अखबार की व्यवस्था संभालने का योग रहा है।” 2
गांधीजी ने आत्मकथा में ‘इंडियन ओपिनियन’ का प्रकाशन वर्ष भूलवश 1904 दिया है। ‘इंडियन ओपिनियन’ 1904 में नहीं, 1903 में निकला था। मनसुखलाल नाजर पर संपादन का सच्चा भार भले न हो, उनके प्रति गांधीजी ऊंची श्रद्धा रखते थे। गांधीजी ने लिखा है, “मनसुखलाल नाजर संपादक का काम न कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने देश में कई अखबारों के लिए लेख लिखे थे, पर दक्षिण अफ्रीका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे रहते उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें मेरी विवेक-शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। अतएव जिन-जिन विषयों पर कुछ लिखना जरूरी होता, उन पर लिखकर भेजने का बोझ वे मुझ पर डाल देते थे।”3गाधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ की पहली संपादकीय का शीर्षक दिया था ‘आवरसेल्व्स’। उसका गुजराती, हिंदी और तमिल खंडों में अनुवाद भी छपा था। हिंदी अनुवाद अपनी बात शीर्षक से छपा था। उसमें गांधीजी ने उस समाचार पत्र की आवश्यकता और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लिखा था, “इस समाचार पत्र की जरूरत के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। भारतीय समाज दक्षिण अफ्रीका के राजकीय शरीर का निर्जीव अंग नहीं है; इसलिए उसकी भावनाओं को प्रकट करनेवाले और विशेष रूप से उसके हित में संलग्न समाचार पत्र का प्रकाशन अनुचित नहीं समझा जाएगा। बल्कि हम समझते हैं कि उससे एक बड़ी कमी पूरी होगी।” 4 प्रवेशांक में ही गांधीजी ने ‘दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश भारतीय’ शीर्षक टिप्पणी में रंगभेद के प्रश्न को शिद्दत से उठाते हुए लिखा था, “दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी सामाजिक और अन्य अन्य तमाम दृष्टियों से अछूत से बने हुए हैं; कहीं कम, कहीं ज्यादा। वहां उन्हें तिरस्कारपूर्वक कुली कहा जाता है। वास्तव में वहां के लोग साधारणतया गंदे जीव मानते हैं जिनमें किसी सद्गुण का लेश मात्र भी नहीं हो सकता।”
‘इंडियन ओपिनियन’ पहले चार भाषाओं- अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिन्दी में प्रकाशित होता था। बाद में तमिल और हिन्दी संस्करण बंद कर दिए गए। उसका कारण गांधीजी ने इस प्रकार बताया है, “तमिल और हिन्दी का बोझ हर तरह से अधिक लगने के कारण, खेत पर रह सकें, ऐसे तमिल और हिन्दी लेखक न मिलने के कारण और इन दो भाषाओं के लेखों पर अंकुश न रह सकने के कारण वे दो विभाग बन्द कर दिए गए और अंग्रेजी तथा गुजराती विभाग जारी रखे गए।” 6 अखबार में घाटा को रोकने के लिए उसमें काम करने वाले लोगों को साझेदार या साझेदार जैसा बनाकर एक खेत खरीद कर उसमें उन सबको बसाया गया। वह खेत डरबन से 13 मील दूर एक पहाड़ी पर था। उसके निकट का फिनिक्स रेलवे स्टेशन खेत से 3 मील दूर था। गांधीजी ने लिखा है, “सत्याग्रह की लड़ाई शुरू हुई, तब गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में ‘इंडियन ओपिनियन’ निकलता था। खेत पर बस कर संस्था में काम करने वाले लोगों में गुजराती, हिन्दी भाषी (उत्तर भारतीय), तमिल और अंग्रेज सभी थे। श्री मनसुखलाल नाजर की असामयिक मृत्यु के बाद एक अंग्रेज मित्र हर्बर्ट किचन ‘इंडियन ओपिनियन’ के संपादक बने। उनके बाद संपादक के पद पर श्री हेनरी पोलाक ने लम्बे समय तक कार्य किया। मेरे और श्री पोलाक के जेल-निवास के दिनों में भले पादरी जोसफ डोक अखबार के संपादक रहे।” 7 ‘इंडियन ओपिनियन’ ने क्या कार्य किए और किस तरह वह सत्याग्रह की लड़ाई का साधन बना, इसका वृत्तांत भी गांधीजी ने दिया है, “इस अखबार के द्वारा कौम के लोगों को हर सप्ताह के संपूर्ण समाचारों से अच्छी तरह परिचित रखा जा सकता था। साप्ताहिक के अंग्रेजी विभाग द्वारा ऐसे हिन्दुस्तानियों को सत्याग्रह की थोड़ी-बहुत तालीम मिलती थी, जो गुजराती नहीं जानते थे और हिन्दुस्तान, इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों के लिए तो ‘इंडियन ओपिनियन’ एक साप्ताहिक समाचार पत्र की गरज पूरी करता था। मेरा यह विश्वास है कि जिस लड़ाई का मुख्य आधार आंतरिक बल पर है, वह लड़ाई अखबार के बिना लड़ी जा सकती है परन्तु इसके साथ मेरा यह अनुभव भी है कि ‘इंडियन ओपिनियन’ के होने से हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं, कौम को आसानी से सत्याग्रह की शिक्षा दी जा सकी और दुनिया में जहां कहीं भी हिन्दुस्तानी रहते थे, वहां सत्याग्रह सम्बन्धी घटनाओं के समाचार फैलाए जा सके। यह सब अन्य किसी साधन से शायद संभव न होता। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने के साधनों में ‘इंडियन ओपिनियन’ भी एक अत्यन्त उपयोगी और प्रबल साधन था।” 8 गांधी जी का दृढ़ मत था कि अखबार विज्ञापन के बल पर नहीं, अपितु ग्राहकी के बल पर चलाया जाना चाहिए। ‘इंडियन ओपिनियन’ के ही संदर्भ में उन्होंने लिखा है, “पहले उस साप्ताहिक में विज्ञापन लिए जाते थे। प्रेस में बाहर का फुटकर काम भी छापने के लिए स्वीकार किया जाता था। मैंने देखा कि इन दोनों कामों में हमारे अच्छे से अच्छे आदमियों को लगाना पड़ता था। विज्ञापन लेने ही हों तो कौन से विज्ञापन लिए जाएं और कौन से न लिए जाएं, इसका निर्णय करने में हमेशा ही धर्म संकट खड़े होते थे। इसके सिवा, किसी आपत्तिजनक विज्ञापन को न लेने का मन हो, परन्तु विज्ञापन देने वाला कौम का कोई अग्रगण्य व्यक्ति हो, तो उसके बुरा मान जाने के भय से भी हमें न लेने योग्य विज्ञापन लेने के प्रलोभन में फंसना पड़ता था। विज्ञापन प्राप्त करने में और छपे हुए विज्ञापनों के पैसे वसूल करने में हमारे अच्छे से अच्छे आदमियों का समय खर्च होता था और विज्ञापनदाताओं की खुशामद करनी पड़ती सो अलग। इसके साथ यह विचार भी आया कि यदि अखबार पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि केवल कौम की सेवा के लिए ही चलाना हो, तो वह सेवा जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कौम चाहे तो ही उसकी सेवा हमें करनी चाहिए। और कौम की इच्छा का स्पष्ट प्रमाण यही माना जाएगा कि कौम के लोग काफी बड़ी संख्या में साप्ताहिक के ग्राहक बनकर उसका खर्च उठा लें। इसके सिवा, हमने यह भी सोचा कि अखबार चलाने के लिए उसका मासिक खर्च निकालने की दृष्टि से कुछ व्यापारियों को सेवाभाव के नाम पर अपने विज्ञापन देने की बात समझाने की अपेक्षा यदि कौम के आम लोगों को ‘इंडियन ओपिनियन’ खरीदने का कर्तव्य समझाया जाए तो वह ललचाने वाले लोगों और ललचाये जाने वाले लोगों दोनों के लिए कितनी सुन्दर शिक्षा हो सकती है? इन सारी बातों पर हमने सोच विचार किया और उस पर तुरन्त अमल भी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कार्यकर्ता विज्ञापन विभाग की झंझटों में फंसे रहते थे, वे अब अखबार को सुन्दर बनाने के प्रयत्नों में लग गए। कौम के लोग तुरन्त समझ गए कि ‘इंडियन ओपिनियन’ की मालिकी और उसे चलाने की जिम्मेदारी दोनों उनके हाथ में है। इसके फलस्वरूप हम सब कार्यकर्ता निश्चिन्त हो गए। कौम अखबार की मांग करे, तब तक उसे निकालने के लिए पूरी मेहनत करने की चिन्ता ही हमारे सिर पर रह गई।” 9 गांधीजी का मानना था कि ग्राहकी के लिए पाठकों से निवेदन करने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने लिखा है, “किसी भी हिन्दुस्तानी का हाथ पकड़ कर उससे ‘इंडियन ओपीनियन’ का ग्राहक बनने की बात कहने में हमें लज्जा नहीं आती थी, बल्कि ऐसा कहना हम अपना धर्म समझते थे। ‘इंडियन ओपिनियन’ की आंतरिक शक्ति में और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ और वह एक महाशक्ति बन गया। उसकी ग्राहक-संख्या, जो सामान्यतः 1200 से 1500 तक रहती थी, दिनों-दिन बढ़ने लगी। उसका वार्षिक चन्दा हमें बढ़ाना पड़ा फिर भी जब सत्याग्रह की लड़ाई ने उग्र रूप धारण किया, उस समय उसके ग्राहकों की संख्या 3500 तक पहुंच गई थी। ‘इंडियन ओपिनियन’ के पाठकों की संख्या अधिक से अधिक 20000 मानी जा सकती हैं। इतने पाठकों के बीच उसकी 3000 से ऊपर प्रतियां बिकना आश्चर्यजनक फैलाव कहा जाएगा।” 10 ‘इंडियन ओपिनियन’ ऐसा अखबार निकला कि पाठक उसका बेसब्री से इंतजार करते थे। गांधीजी ने लिखा है, “कौम ने ‘इंडियन ओपिनियन’ को इस हद तक अपना बना लिया था कि यदि निश्चित समय पर उसकी प्रतियां जोहानिसबर्ग न पहुंचतीं, तो मुझ पर शिकायतों की झड़ी लग जाती थी। प्राय: रविवार को सुबह अखबार जोहानिसबर्ग पहुंच जाता था। मैं जानता हूं कि बहुत से हिन्दुस्तानी अखबार पहुंचने पर सबसे पहला काम उसके गुजराती विभाग को आदि से अंत तक पढ़ जाने का करते थे। एक आदमी पढ़ता था और दस-पन्द्रह आदमी उसके आसपास बैठकर सुनते थे। हम गरीब ठहरे, इसलिए कुछ लोग साझे में भी ‘इंडियन ओपिनियन’ खरीदते थे।” 11
‘इंडियन ओपिनियन’ में विज्ञापन और बाहर से मिलनेवाले फुटकर काम प्रेस में बंद करने का परिणाम अच्छा रहा। गांधीजी ने लिखा है, “प्रेस में बाहर का फुटकर काम लेना उसी तरह बंद कर दिया गया था, जिस तरह विज्ञापन लेना बन्द कर दिया गया था। उसे बन्द करने के कारण प्राय: वैसे ही थे जैसे विज्ञापन न लेने के थे। यह काम बन्द करने से कंपोजिटरों का जो समय बचा, उसका उपयोग प्रेस द्वारा पुस्तकें प्रकाशित करने में हुआ और कौम जानती थी कि पुस्तकें प्रकाशित करने का हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं था। चूंकि ये पुस्तकें केवल लड़ाई को सहायता पहुंचाने के लिए ही छापी जाती थीं, इसलिए उनकी बिक्री भी अच्छी होने लगी। इस प्रकार ‘इंडियन ओपिनियन’ और प्रेस दोनों ने सत्याग्रह की लड़ाई में भाग लिया और यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि जैसे-जैसे सत्याग्रह की जड़ कौम में जमती गई, वैसे-वैसे सत्याग्रह की दृष्टि से साप्ताहिक और उसके प्रेस की नैतिक प्रगति भी होती गई।”12लेकिन नैतिक प्रगति के बावजूद एक समय ‘इंडियन ओपिनियन’ की आर्थिक प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगा था और स्वयं गांधीजी को आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ती थी। गांधीजी नेलिखा है, ‘मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि इस अखबार में मुझे कुछ अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ही समय में मैंने देखा कि अगर मैं पैसे न दूं, तो अखबार चल ही नहीं सकता। मैं अखबार का संपादक नहीं था। फिर भी हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों यह जानने लग गए थे कि उसके लेखों के लिए मैं ही जिम्मेदार था। अखबार न निकलता तो भी कोई हानि न होती। पर निकालने के बाद उसके बंद होने से हिन्दुस्तानियों की बदनामी होगी और समाज को हानि पहुंचेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं उसमें पैसे उड़ेलता गया और कहा जा सकता है कि आखिर ऐसा भी समय आया, जब मेरी पूरी बचत उसी पर खर्च हो जाती थी। मुझे ऐसे समय की याद है, जब मुझे हर महीने 75 पौंड भेजने पड़ते थे।” 13
इन सबके बावजूद सबसे अच्छी बात यह थी कि’इंडियन ओपिनियन’ में अपनी भूमिका को लेकर गांधीजी के मन में गहरा संतोष था। उन्होंने लिखा है, “इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस अखबार ने हिन्दुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वह मेरे अधीन था, उसमें किए गए परिवर्तन मेरे जीवन में हुए परिवर्तनों के द्योतक थे। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उड़ेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप में पहचानता था, उसे समझाने का प्रयत्न करता था। जेल के समयों को छोड़कर दस वर्षों के अर्थात् सन् 1914 तक के ‘इंडियन ओपिनियन’ के शायद ही कोई अंक ऐसे होंगे, जिनमें मैंने कुछ लिखा न हो। इनमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो या किसी को केवल खुश करने के लिए लिखा हो अथवा जान-बूझकर अतिशयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता।” 14 गांधी जी की इस टिप्पणी से आज के पत्रकार यह सीख ले सकते हैं कि उन्हें एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखना चाहिए। न अतिशयोक्ति करनी चाहिए।
गांधीजी पत्रकारों को सीख देते हैं तो पत्रकारिता से स्वयं भी सीखते हैं। ‘इंडियन ओपिनियन’ ने गांधीजी को संयम सिखाया। उन्होंने खुद लिखा है, “मेरे लिए यह अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ था। मित्रों के लिए वह मेरे विचारों को जानने का माध्यम बन गया था। आलोचकों को उसमें से आलोचना के लिए बहुत कम सामग्री मिल पाती थी। मैं जानता हूं कि उसके लेख आलोचकों को अपनी कलम पर अंकुश रखने के लिए बाध्य करते थे। इस अखबार के बिना सत्याग्रह की लड़ाई चल नहीं सकती थी। पाठक समाज इस अखबार को अपना समझकर इसमें से लड़ाई का और दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों की दशा का सही हाल जानता था।” 15 गांधीजी को इसका गहरा बोध था कि अखबार संपादक का नहीं, पाठक का होता है। संपादक और पाठक के संबंध के बारे में गांधीजी ने लिखा है, “इस अखबार के द्वारा मुझे मनुष्य के रंग-बिरंगे स्वभाव का बहुत ज्ञान मिला। संपादक और ग्राहक के बीच निकट का और स्वच्छ सम्बन्ध स्थापित करने की ही धारणा होने से मेरे पास हृदय खोलकर रख देनेवाले पत्रों का ढेर लग जाता था। उसमें तीखे, कड़वे, मीठे यों भांति-भांति के पत्र मेरे नाम आते थे। उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना, उनमें से विचारों का सार लेकर उत्तर देना, यह सब मेरे लिए शिक्षा का उत्तम साधन बन गया था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो इसके द्वारा मैं समाज में चल रही चर्चाओं और विचारों को सुन रहा होऊं। मैं संपादक के दायित्व को भलीभांति समझने लगा और मुझे समाज के लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसके कारण भविष्य में होनेवाली लड़ाई संभव हो सकी, वह सुशोभित हुई और उसे शक्ति प्राप्त हुई।” 16
गांधीजी की पत्रकारिता से पत्रकार यह सीख भी ले सकते हैं कि उन्हें स्वयं पर अंकुश रखना चाहिए। गांधीजी ने लिखा है, “‘इंडियन ओपिनियन’ के पहले महीने के कामकाज से ही मैं इस परिणाम पर पहुंच गया था कि समाचार पत्र सेवा भाव से ही चलाने चाहिए। समाचार पत्र एक जबरदस्त शक्ति है, किन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डूबो देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कलम का निरंकुश प्रवाह भी नाश की सृष्टि करता है। यदि ऐसा अंकुश बाहर से आता है, तो वह निरंकुशता से भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुश तो अंदर का ही लाभदायक हो सकता है। यदि यह विचारधारा सच हो, तो दुनिया के कितने समाचार पत्र इस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं? लेकिन निकम्मों को बंद कौन करे? कौन किसे निकम्मा समझे? उपयोगी और निकम्मे दोनों साथ-साथ ही चलते रहेंगे। उनमें से मनुष्य को अपना चुनाव करना होगा।”17गांधी जी की कसौटी पर खरा नहीं उतरनेवाले जाहिर है कि निरंकुश और निकम्मी पत्रकारिता की श्रेणी में आएंगे।
गांधी जी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ में रंगभेद के प्रश्न को बार-बार और जोर-शोर से उठाया। ‘इंडियन ओपिनियन’ के आठ अक्टूबर 1903 के अंक में उन्होंने लिखा, “क्या हम महामान्य और उनकी सरकार से क्षणभर रुककर सोचने के लिए नहीं कह सकते? घोषणा से इतना तो प्रकट है कि हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। जिस हृदय में ऐसी श्रद्धा निवास करती है, क्या उसके लिए एक समस्त जाति को, महज इसलिए कि उसकी चमड़ी का रंग उस व्यक्ति की चमड़ी के रंग से जुदा है, निंदित बताना सुसंगत है, जबकि दोनों एक ही राजा के प्रति राजभक्ति के बंधनों से बंधे हैं? क्या ब्रिटिश भारतीयों ने ऐसी कोई बुराई की है जिससे उन्हें इतना अपमानित करना उचित हो जितने कि उपनिवेश में किए जाते हैं? किंतु अश्वेत लोगों के प्रति इस जिहाद को जारी ही रखना है तो झूठमूठ विनय का नाम लेकर प्रार्थना के लिए मुकर्रर करके ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध क्यों करते हैं?”18गांधी जी ने ‘इंडियन ओपिनियन’, 16-04-1904 के अंक में रंगभेद के प्रश्न को फिर उठाया। उन्होंने लिखा, “आरेंज रिवर उपनिवेश के 31 मार्च के गजट में कहा गया है कि कोई भी गाड़ी का मालिक जो अपनी गाड़ी को केवल अश्वेत यात्रियों को ही ले जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, टाउन क्लार्क से एक तख्ती प्राप्त कर सकता है जिस पर अश्वेत यात्रियों के लिए शब्द साफ तौर पर छपे होंगे। किसी भी अश्वेत व्यक्ति को सिवा उन रजिस्टर्ड गाड़ियों के जो इस काम के लिए अलग की गई हों और जिन पर पहचान के लिए पहले बताई गई रंगीन तख्ती हो, किसी रजिस्टर्ड गाड़ी में सफर नहीं करने दिया जाएगा।” 19 इतनी सूचना देने के बाद गांधीजी लिखते हैं, “अश्वेत लोगों के विरुद्ध आरेंज रिवर उपनिवेश की सरकार के दुराग्रही रवैये की हमने इतनी बार चर्चा की है कि अपनी बात पर जोर देने के लिए हम उपर्युक्त अंशों की ओर अपने पाठकों का केवल ध्यान आकर्षित कर देते हैं। अधिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है।”20इसी तरह गांधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ के 12-11-1903 के अंक में लिखा, “ट्रांसवाल सरकार ने अभी हाल ही में सभी अश्वेत लोगों का नगरपालिका के चुनाव में भाग लेने के अधिकार छीन लिया है। ब्रिटिश भारतीयों पर यह पाबंदी निश्चित ही उन पर लगी पाबंदियों में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है किंतु हम इसे ब्रिटिश भारतीयों के विरुद्ध सरकार की जान-बूझकर अख्तियार की गई द्वेषपूर्ण नीति के रूप में देखते हैं।” 21
गांधीजी को इसका बहुत क्षोभ था कि दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश सरकार बहुत कम सुननेवाली थी। उन्होंने ‘इंडियन ओपिनियन’ के 21-01-1904 के अंक में लिखा, “एक भारतीय कहावत है, रोये बिना माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। फिर ब्रिटिश सरकार तो और भी कम सुननेवाली है। इसलिए हम आशा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीकाभर में हमारे देशवासी ब्रिटिश संविधान के इस पहलू का सावधानी से ध्यान रखेंगे और जब तक पूरा न्याय नहीं होता, तब तक चैन नहीं लेंगे।” 22
गांधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ की पत्रकारिता को लोकोपयोगी बनाने के लिए हरसंभव यत्न किए। उन्होंने उस समय के प्रेरक व्यक्तित्वों पर लेख लिखे। ‘इंडियन ओपिनियन’ के 06-08-1904 के अंक में गांधीजी ने सर फिरोज शाह मेहता पर लेख प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, “डाक से आए समाचार पत्रों से यह अत्यंत आनन्ददायक समाचार मिला है कि माननीय श्री फिरोजशाह मेहता को ‘सर’ की उपाधि प्रदान की गई है। अगर कोई व्यक्ति इस सम्मान का पात्र था तो वे निश्चय ही सर फिरोजशाह हैं। उनकी गिनती सबसे पुराने लोक-सेवकों में है। वे बम्बई नगर-निगम के जनक हैं और शायद उस महान निगम का कोई भी अन्य सदस्य उतनी बैठकों में शामिल नहीं हुआ है, जितनी में वे हुए हैं। सर फिरोज शाह मेहता की तरह उतने लम्बे समय तक निगम की सेवा भी किसी अन्य सदस्य ने न की होगी। वे बम्बई महाप्रान्त के बेताज बादशाह हैं और प्रथम नेता माने जाते हैं। भारत के अन्य किसी प्रान्त में किसी भी अन्य व्यक्ति को यह सम्मान प्राप्त नहीं है। उनको अपनी बेमिसाल योग्यता और अनुभव, प्रभावपूर्ण वक्तृत्वकला, व्यवहार-कुशलता और विरोधियों के प्रति अचूक शिष्टता के फलस्वरूप जनता में बड़ी लोकप्रियता और सरकार में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उन्होंने बम्बई महाप्रान्त के कई कानूनों पर अपनी छाप डाली है, और कलकत्ता-स्थित इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल में सेवा का जो थोड़ा-सा मौका उन्हें मिला, उसमें भी अपने लिए एक अनोखा स्थान बना लिया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सर फिरोजशाह मेहता राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमेशा सम्बद्ध रहे हैं और दो बार उस संस्था के अध्यक्ष भी बने हैं। इसलिए उनका ‘सर’ बनाया जाना उन माननीय महानुभाव का जितना सम्मान है, उतना ही कांग्रेस का भी है। हमारा खयाल है कि सरकार ने उनका सम्मान करके खुद अपना सम्मान किया है। किसी कांग्रेस नेता का इस तरह सम्मान पहली ही बार नहीं किया गया है। माननीय श्री गोखले को भी अभी हाल में सी.आई.ई. का खिताब दिया गया है। जैसा कि पाठकों को मालूम है, माननीय गोखले इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल में महत्वपूर्ण सेवा करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि हाल ही में खिताब पानेवालों में माननीय शंकरन् नायर का भी नाम है। ये सब शायद समय के सूचक चिह्न हैं। मगर साथ ही इनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार उस अच्छे काम से जो भारतीय समाज के नेताओं द्वारा भारत के भिन्न भिन्न भागों में उसके लिए किया जा रहा है, पूरी तरह परिचित है।” 23
‘इंडियन ओपिनियन’ के 03-09-1910 के अंक में गांधी जी ने ‘द ग्रैंड ओल्डमैन आफ इंडिया’ शीर्षक मोनोग्राफ में दादाभाई नौरोजी का संक्षिप्त जीवन दे दिया है। उसमें गांधीजी ने लिखा है, “श्री दादाभाई नौरोजी भारतीयों में ब्रिटिश संसद के सबसे पहले सदस्य थे। उनका जन्म सितम्बर 4, 1825 को बम्बई नगर में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा एनफिन्स्टन सकूल और कॉलेज में हुई और 29 वर्ष की अवस्था में गणित तथा भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बना दिए गए। यह सम्मान पानेवाले पहले भारतीय भी वे ही थे। सन् 1855 में श्री नौराजी इंग्लैंड में स्थापित होनेवाली प्रथम भारतीय व्यावसायिक संस्था के एक साझेदार के रूप में इंग्लैंड गए। लन्दन के यूनिवर्सिटी कॉलेज ने उनको गुजराती का प्रोफेसर नियुक्त करके सम्मानित किया। श्री नौरोजी ने भारत के लिए जो अनेक सुविधाएँ प्राप्त कीं, उनमें से एक थी, 1870 में भारतीयों को प्रशासनिक सेवा (सिविल सर्विस) में प्रवेश करने की अनुमति। सन् 1874 में वे बड़ोदरा के प्रधानमन्त्री हुए और उसके एक वर्ष बाद ही वे बम्बई निगम और नगरपालिका परिषद के सदस्य चुने गए। इस संस्था की उन्होंने पाँच वर्ष तक बहुमूल्य सेवा की। श्री नौरोजी 1885 से 1887 तक बम्बई विधान-परिषद् के सदस्य रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष पद पर चुनकर उनको सम्मानित किया। श्री नौरोजी लन्दन के सेन्ट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र के उदारदलीय प्रतिनिधि के रूप में 1893 से 1895 तक ब्रिटिश लोक-सभा में रहे; और भारतीय व्यय इत्यादि से सम्बन्धित शाही आयोग (रॉयल कमीशन) के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने देश के लिए काफी काम किया। सन् 1897 में उन्होंने वेलबी आयोग के सामने बयान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेस ने जो ब्रिटिश समिति स्थापित की थी, उसके वे प्रारंभ से ही एक उदयमशील सदस्य और कर्मठ कार्यकर्ता रहे। श्री दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तकें लिखीं, वे ये हैं: ‘इंग्लैड्स डयूटी टू इंडिया’ ‘एडमिशन ऑफ एज्यूकेटेड नेटिव्ज इनटू द इंडियन सिविल सर्विस’; ‘फाइनेन्शियल ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया’; और ‘पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रुल इन इंडिया’, यह अंतिम पुस्तक उनकी कृतियों में कदाचित् सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सन 1906 में आदरणीय दादाभाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए स्वदेश-यात्रा की। इसमें उन्हें जो परिश्रम करना पड़ा, वह उन जैसे लौह-शरीर और अदम्य उत्साहशील व्यक्ति के लिए भी बहुत अधिक सिद्ध हुआ। सन् 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद श्री दादाभाई ने सार्वजनिक जीवन से लगभग अवकाश ले लिया, और सन् 1907 में वरसोवा में जाकर बस गए। वरसोवा बम्बई में मछुआरों का एक छोटा-सा गांव है। वहा बैठे हुए वे अब भी भारत के भविष्य को बनाने अथवा बिगाड़नेवाली घटनाओं को गहरी दिलचस्पी के साथ देखा करते हैं। उन्हें जो ‘भारत के पितामह’ कहकर सम्मानित किया जाता है सो नि:सन्देह सर्वथा उचित है।” 24
गांधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ में दुनिया भर के महान व्यक्तियों के मोनोग्राफ भी लिखे। ‘इंडियन ओपिनियन’ में 1905 के विभिन्न अंकों में टालस्टाय, अब्राहम लिंकन, फ्लोरेंस नाइटिंगल, इलिजाबेथ फ्राइ, इश्वरचंद्र विद्यासागर और जार्ज वाशिंगटन के मोनोग्राफ छपे। गांधीजी एक तरफ मोनोग्राफों में यह बताते हैं कि इन महापुरुषों से क्या प्रेरणा ली जा सकती है, तो दूसरी तरफ वे छोटी-छोटी सामान्य चीजों के प्रति भी पाठकों को सचेत करते हैं। पाठकों को सेहत के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से गांधीजी ने 1904 में ‘इंडियन ओपिनियन’ में आहार विज्ञान पर क्रमबद्ध लेख लिखे थे। 1904 में ही गांधीजी ने जान रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक ‘अन टू दिस लास्ट’ पढ़ी। उन्होंने उसका गुजराती में ‘सर्वोदय’ शीर्षक से अनुवाद प्रकाशित किया। गांधीजी ने ‘इंडियन ओपिनियन’ के जनवरी-फरवरी 1907 के अंकों में नैतिक धर्म पर धारावाहिक आठ लेख प्रकाशित किए।
‘इंडियन ओपिनियन’ को सत्याग्रह शब्द का संधान करने का श्रेय भी जाता है। ‘इंडियन ओपिनियन’ के 11 जनवरी 1908 के अंक में जोहानिसबर्ग लेटर नामक स्तंभ में ‘पैसिव रेजिस्टेंस’ के लिए समानार्थी गुजराती शब्द सुझाने के लिए पाठकों से प्रस्ताव मांगे गए। ‘इंडियन ओपिनियन’ के सात मार्च 1908 को यह जानकारी दी गई, “सिर्फ चार व्यक्तियों ने नाम भेजा है। इसमें से हमें सिर्फ एक नाम उपयुक्त लगता है। वह है सत्याग्रह।” पहले सदाग्रह नाम का सुझाव आया था जिसे बदलकर सत्याग्रह कर दिया गया। उस नाम का सुझाव देने वाले मगनलाल गांधी थे। गांधीजी ने टालस्टाय के पत्र एक हिंदू के नाम को ‘इंडियन ओपिनियन’ के 25-12-1909 के अंक में प्रकाशित किया। गांधीजी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय एस.एस. किल्डोनन कासल जहाज में 13 नवंबर 1909 को ‘हिंद स्वराज’ पुस्तक लिखी। उसमें बीस अध्याय हैं। पहले 12 अध्याय पहली बार ‘इंडियन ओपिनियन’ के 11 दिसंबर 1909 के अंक में और शेष अध्याय 18 दिसंबर 1909 के अंक में छपे। पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। जब वह पुस्तक भारत में प्रतिबंधित की गई तो गांधीजी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ‘इंडियन ओपिनियन’ के 2 अप्रैल 1910 में गांधीजी ने लिखा था, “‘हिंद स्वराज’ में व्यक्त विचार मेरे हैं लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक इसे तैयार करने में भारतीय दार्शनिकों के अलावा टालस्टाय, रस्किन, थोरो, इनरसन और अन्य लेखकों को शामिल करने का प्रयास किया है।” गांधीजी को लिखे गए टालस्टाय के पत्र ‘लेटर टू ए हिंदू’ का प्रकाशन ‘इंडियन ओपिनियन’ के 25 दिसंबर 1909, एक जनवरी 1910 और 8 जनवरी 1910 के अंकों में हुआ।
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर भारतवंशियों को अधिकार दिलाने के बाद गांधीजी भारत के लिए रवाना हुए। भारत के लिए रवाना होने के पहले उन्होंने कैपटाउन में रायटर के संवाददाता को एक पत्र सौंपा जो दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों और यूरोपीय समुदाय को संबोधित था। वह पत्र ‘इंडियन ओपिनियन’ के 29 जुलाई 1914 के अंक में ‘फेयरवेल लेटर’ शीर्षक से छपा। उसमें गांधीजी ने कहा था, “दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और यूरोपीय समुदाय के लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया, वह मुझ पर कर्ज है और कर्जदार के रूप में मैं भारत जा रहा हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं आगे भी सत्य और केवल सत्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा।
यह लेख प्रो. कृपाशंकर चौबे द्वारा गांधी की पत्रकारिता पर लिखी गई है।
![]()
Discover more from जन विचार
Subscribe to get the latest posts sent to your email.