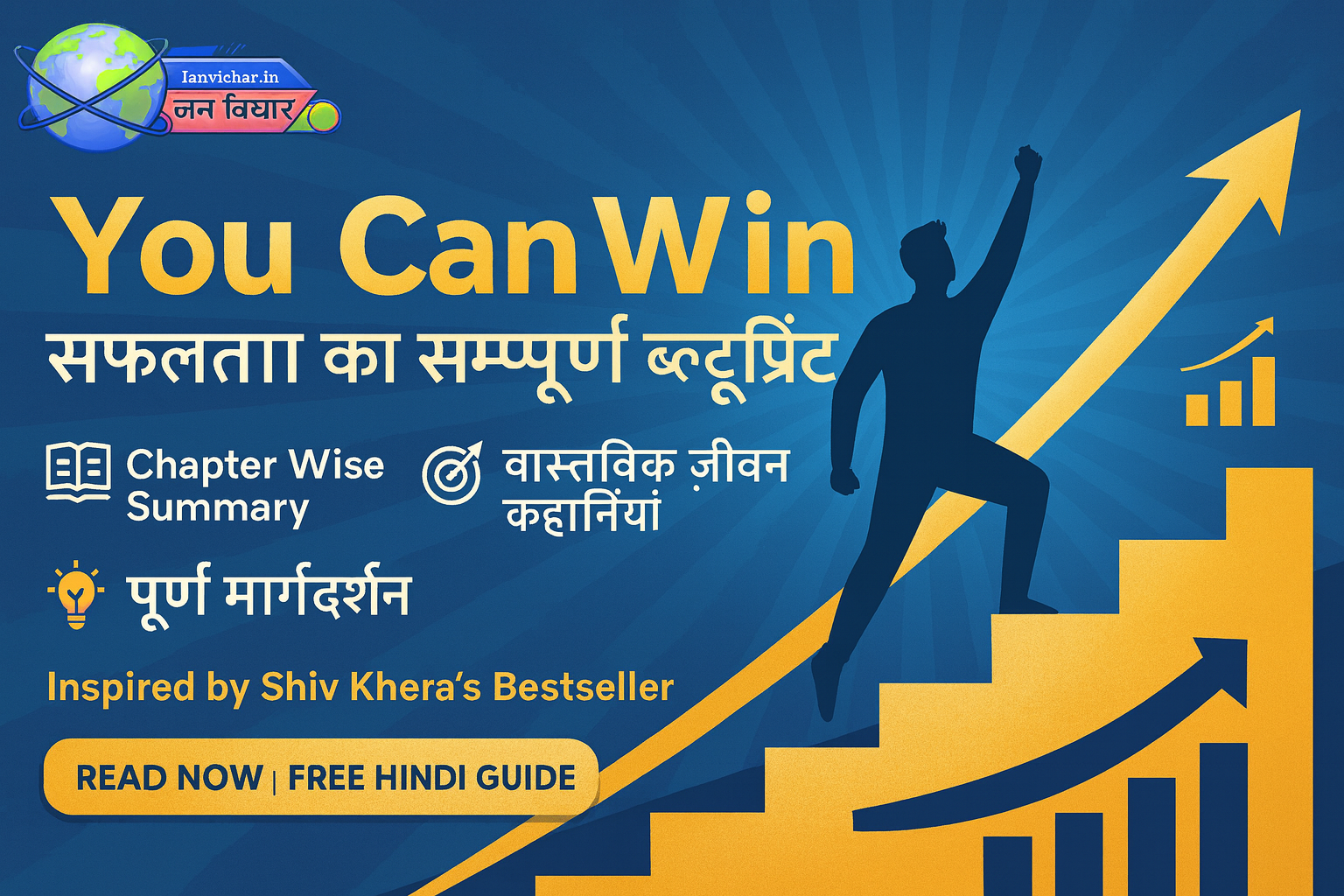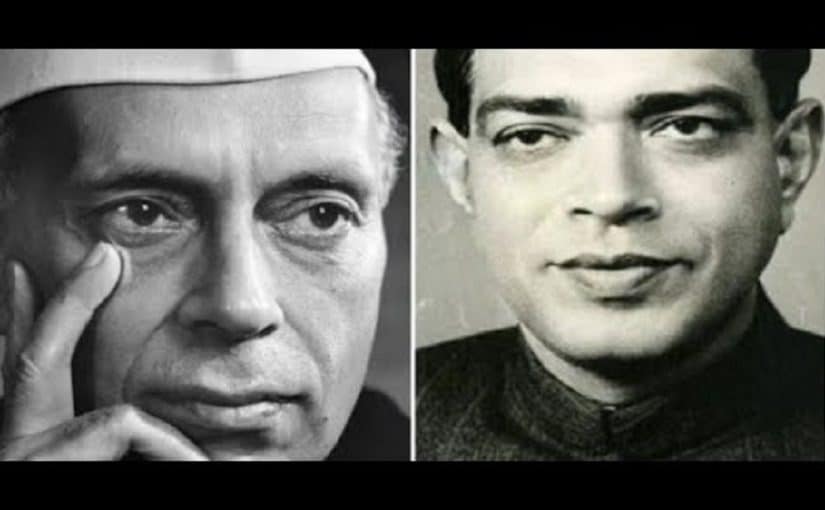
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर (1908-1962) शौर्य एवं सामाजिक पीड़ा के आवेश और पूर्ण स्वाधीनता की अभिलाषा के रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की यथार्थ तस्वीर दिखती है। आरंभिक समय से ही उन्होंने राष्ट्र के जीवन, राष्ट्र की संवेदना तथा समकालीन राजनीतिक चेतना में आ रहे परिवर्तनों को सजगता के साथ रूपायित किया। शुरू से अंत तक उनकी पक्षधरता शोषित- पीड़ित जनता के साथ रही। उनकी काल चेतना में वैसे समाज की कल्पना झलकती है जहाँ उत्पीड़न और असमानता की जगह न हो। शोषण मुक्त समाज का निर्माण उनका वैचारिक पक्ष था। उनके संपूर्ण रचना संसार में इन सभी प्रतिबद्धताओं की झलक दिखाई देती है। रामधारी सिंह दिनकरः संकलित निबंध शीर्षक यह पुस्तक संपूर्ण दिनकर के वैचारिक स्रोत को देखने की प्रेरणा देती है।
हिन्दी के ‘उर्वशी’, ‘कुरुक्षेत्र’ और ‘रश्मिरथी’ समेत 33 काव्य- कृतियों के रचयिता और ‘राष्ट्रकवि’ के विशेषण से विभूषित डॉ. रामधारी सिंह ‘दिनकर’ एक उत्कृष्ट गद्यकार भी थे। उनकी पुस्तकों की कुल संख्या 60 बताई जाती है, जिनमें सत्ताइस गद्यग्रंथ हैं। इनमें आधी पुस्तकों में निबंध या निबंध के ढंग की चीजें संकलित हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्रम है- मिट्टी की ओर (1946), अर्धनारीश्वर (1952), रेती के फूल (1954), हमारी सांस्कृतिक एकता (1954), राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता (1958), ९ काव्य की भूमिका (1958), पंत, प्रसाद और मैथिली शरण (1958), वेणुवन (1958), धर्म, नैतिकता और विज्ञान (1959), वर-पीपल (1961), शुद्ध कविता की खोज (1966), साहित्यमुखी (1968), भारतीय एकता (1970), आधुनिक बोध (1973), विवाह की मुसीबतें (1974) आदि। इनके अतिरिक्त देश-विदेश (1957), लोकदेव नेहरू (1965), राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी (1968) जैसी कृतियां भी हैं, जिनमें यात्रा-वृतांत व संस्मरण आदि के बीच-बीच में वैचारिक निबंध गुम्फित हैं।
दिनकर जी सन् 1940 के आसपास गद्य ९ लेखन की ओर गंभीरता से प्रवृत्त हुए। उनका पहला संकलन ‘मिट्टी की ओर’ 1946 में प्रकाशित हुआ। जबकि कविता लेखन वे 15-16 वर्ष की अवस्था से ही करने लगे थे। उस समय वे माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे।
उनकी पहली कविता 1924-25 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका ‘छात्र-सहोदर’ में छपी थी। दिनकर की पहली काव्य पुस्तक ‘प्रण-भंग सन् 1929 में प्रकाशित हुई थी। यह ‘महाभारत’ के कथानक पर आधारित थी। इस समय उनकी अवस्था 21 वर्ष की थी। पद्य से गद्य की ओर प्रवृत्त होने में दिनकर जी ने लगभग 20 वर्षों का समय लिया। प्राचीन मनीषियों ने भी गद्यं कवीणां निकषं वदन्ति ! अनुमान होता है कि दिनकर ने लगभग दो दशकों की काव्य-साधना के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ गद्य के क्षेत्र में प्रवेश लिया। तभी तो उनका गद्य इतना प्रगल्भ, परिमार्जित और प्रभावोत्पादक बन पड़ा है। बाद की पीढ़ियों के कवियों-लेखकों के लिए यह एक अनुकरणीय बात है। वर्ष 1958-59 में दिनकर का गद्य-लेखन अपने उत्कर्ष पर था। इस साल उनके 5 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। ‘मिट्टी की ओर’ उनका पहला और ‘विवाह की मुसीबतें’ अंतिम निबंध संकलन माना जाता है। इस संबंध में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लेखक का विवाह 1920-21 में हुआ था जब उनकी अवस्था 13 वर्ष की थी। लेकिन विवाह की मुसीबतें नामक यह संकलन सन् 1974 में अर्थात उनके विवाह के लगभग 54 वर्ष बाद प्रकाश में आया। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती श्यामवती थी।
हिन्दी के विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के बीच भी रामधारी सिंह ‘दिनकर’ का कवि रूप ही अधिक उजागर है। जबकि उनका गद्यकार रूप भी कम उज्जवल नहीं है। उनके निबंधों का यह संकलन तैयार करवाकर नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। इसके लिए दिनकर के सभी प्रेमियों को ट्रस्ट का आभारी होना चाहिए।
रचना संसार के साथ-साथ दिनकर का जीवन वृत्त भी दिलचस्प है। पाठकों को उनके निबंधों में व्यक्त विचारों और भावनाओं की पृष्ठभूमि को समझने में उनके जीवन वृत्त से सहूलियत होगी। हिन्दी साहित्याकाश के अपने समय के इस जाज्वल्यमान नक्षत्र की दीप्ति समय के अंतराल के साथ कुछ अर्चिचत-सी हो गई है।
रामधारी सिंह ‘दिनकर’ का जन्म बिहार प्रदेश के बेगूसराय (पुराने मुंगेर) जिले के सिमरिया गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय भूमिहार ब्राह्मण किसान परिवार में 23 सिंतबर 1908 को हुआ था। यह ग्राम पुण्यतोया गंगा नदी के पावन उत्तरी तट पर बसा हुआ है। और मिथिलाचंल का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां पूरे उत्तर बिहार समेत नेपाल से तीर्थ यात्री बड़ी संख्या में आते हैं और प्रति वर्ष कार्तिक माह कल्पवास चलता है। किंवदंती यह है कि विवाहोपरांत सीता को विदा कराकर ले जाते समय राम ने इसी स्थान पर गंगा को पार किया था। तभी से यह स्थान सिमरियाघाट के नाम से प्रसद्धि है। इस नाम में से ‘म’ और ‘रि’ को हटा दें तो वह ‘सियाघाट’ हो जाता है। 1 दिसंबर 1973 को जब दिनकर जी को ‘उर्वशी’ के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था, तब अपने उद्बोधन में उन्होने कहा था-भगवान ने मुझको जब इस पृथ्वी पर भेजा तो मेरे हाथ में एक हथौड़ा दिया और कहा कि जा तू इस हथौड़े से चट्टान के पत्थर तोड़ेगा और तेरे तोड़े हुए अनगढ़ पत्थर भी कला के समुद्र में फूल के समान तैरेंगे।…. मैं रंदा लेकर काठ को चिकनाने नहीं आया था। मेरे हाथ में तो कुल्हाड़ा था जिससे मैं जड़ता की लकड़ियों को फाड़ रहा था।…. अपने प्रशंसकों के बीच, जिनमें इन पंक्तियों के लेखक से लेकर स्व. जवाहरलाल नेहरू तक शामिल हैं, दिनकर, पौरुष और ललकार के कवि माने जाते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जैसे प्रशंसा-कृपण आलोचकों ने भी उन्हें उद्बोधन का कवि माना है।
दिनकर जब दो साल के थे तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया। उनके अग्रज और अनुज-दोनों ने इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और किसानी में लग गए ताकि दिनकर की पढ़ाई निर्बाध गति से चलती रहे। तेरह वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास की। उनका काव्य-सृजन इसी समय शुरू हुआ।
दिनकर की कोई 32 काव्य कृतियां एक-एक कर प्रकाश में आईं। लेकिन ‘उर्वशी’ (1961) महाकाव्य को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, उसके लिए सन् 1973 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी गद्य रचना ‘संस्कृति के चार अध्याय’ के लिए उन्हें सन् 1959 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। इनकी कई रचनाओं का अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
उनका व्यक्तिगत जीवन संघर्षों, उपलब्धियों और दायित्वों से भरा रहा। स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। सन् 1934 में सरकारी नौकरी में गए और सन् 1942 तक सब-रजिस्ट्रार के पद पर रहे, जमीन-जायदाद और शादी-ब्याह से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन करना था। सन् 1947 में वे बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक बने। इसके बाद से उनके जीवन में पदों और सम्मानों की बाढ़ सी आ गई।
स्नातकोत्तर उपाधि से रहित होने के बावजूद उन्हें महाविद्यालय में हिन्दी का अध्यापक नियुक्त किया गया। यह उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभा का सम्मान था। बारह वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। इसके बाद भारत सरकार के गृहमंत्रालय में हिन्दी सलाहकार मनोनीत हुए। सन् 1971 में वे सारे पदभारों से मुक्त होकर पटना चले आए।
इस बीच सन् 1959 में उन्हें ‘पद्मभूषण की उपाधि प्रदान की गई। सन् 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, पश्चिम जर्मनी और रूस के साथ-साथ चीन, मिस्त्र और मॉरीशस आदि देशों का भी भ्रमण किया। इस क्रम में बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और राजनेताओं से उनकी निकटता बढ़ी।
इस बीच सन् 1959 में उन्हें ‘पद्मभूषण की उपाधि प्रदान की गई। सन् 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी. लिट. की मानद उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, पश्चिम जर्मनी और रूस के साथ-साथ चीन, मिस्त्र और मॉरीशस आदि देशों का भी भ्रमण किया। इस क्रम में बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और राजनेताओं से उनकी निकटता बढ़ी।
इस पूरे दौर में एक भरे-पूरे संयुक्त परिवार का दायित्व उनके कंधों पर रहा। उन्होंने अपने हाथों दस कन्याओं का विवाह रचाया, जिसमें उनकी दो पुत्रियां, छह भतीजियां तथा दो पोतियां शामिल हैं। इसको वे अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते थे।
![]()
Discover more from जन विचार
Subscribe to get the latest posts sent to your email.