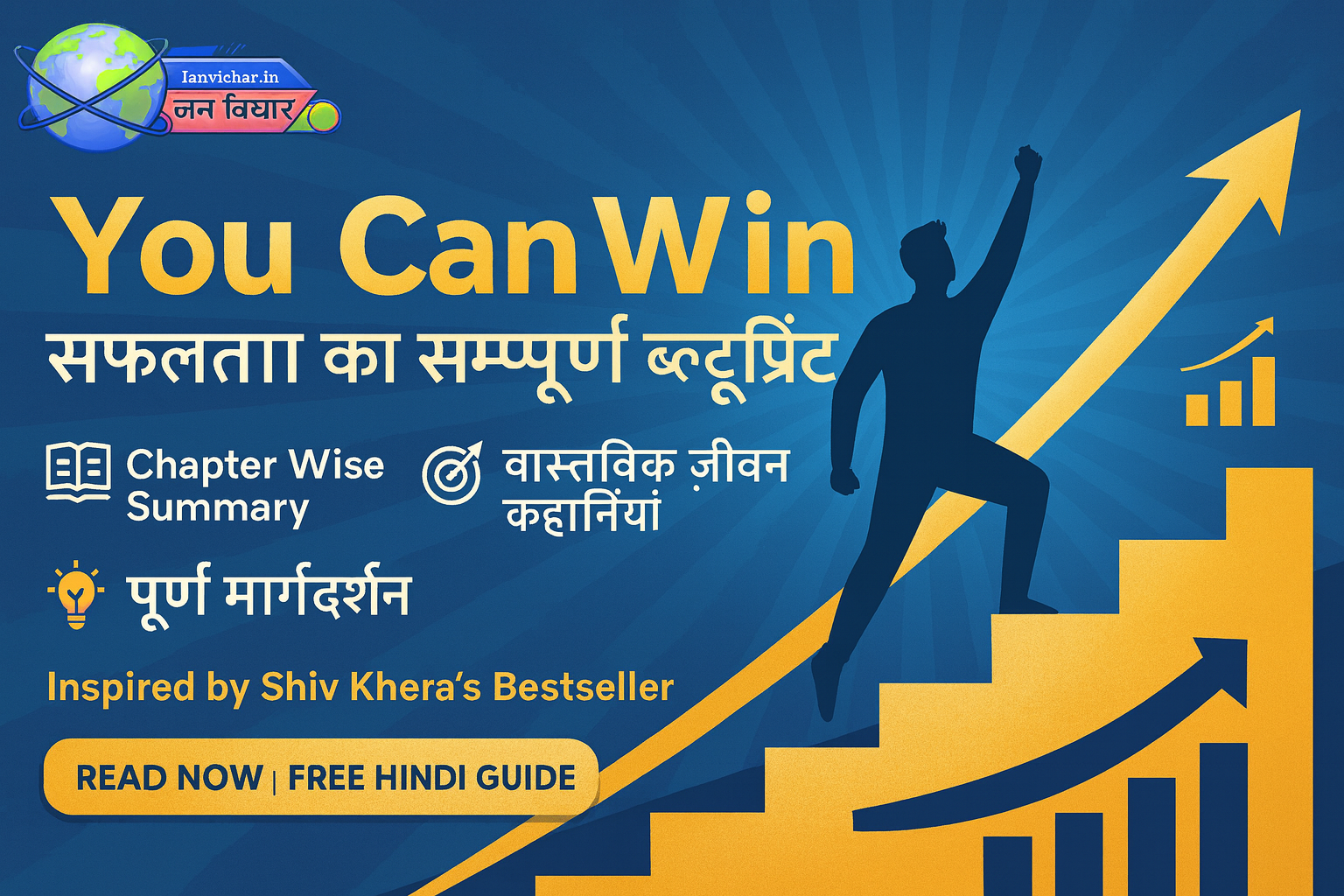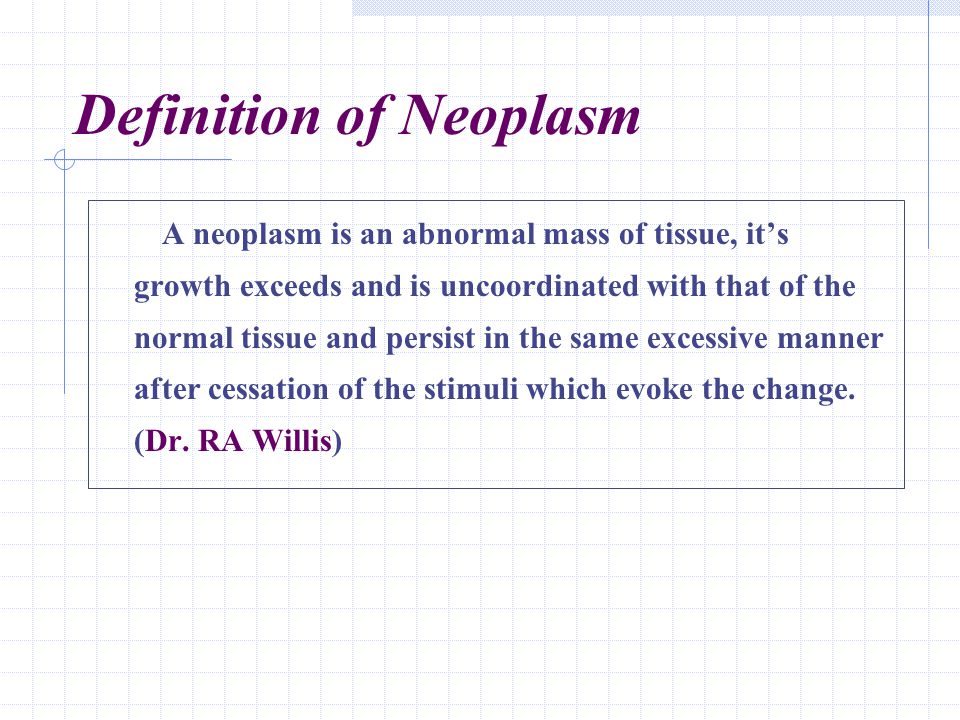
तेज़ी से बदलती दुनिया, लगातार आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा के जीवन में आते जा रहे बदलाव। हमारा दिमाग़ इन सब कामों के लिए नहीं बना था, जो आज हम करते हैं. फिर भी हम इस आधुनिक दुनिया में अच्छे से ढल गए हैं और लगातार आ रहे बदलावों के हिसाब से ख़ुद को बदलते भी जा रहे हैं। ये सब संभव हो पाया है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के कारण. एक ऐसा अंग जिसमें ख़ुद को ढालने, सिखाने और विकसित करने की ज़बरदस्त क्षमता है।सवाल उठता है कि हम इस कमाल के अंग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीक़ा है जिससे हम मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाकर इसे तेज़-तर्रार बना सकते हैं ?
बीबीसी की विज्ञान पत्रकार मेलिसा होगेनबूम ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए नए शोधों का अध्ययन किया और कुछ विशेषज्ञों से बात की।
इंग्लैंड की सरे यूनिवर्सिटी में क्लीनिकल साइकोलॉजी के प्रोफ़ेसर थॉरस्ट्रीन बार्नहोफ़र ने मेलिसा को बताया कि हम अपने दिमाग़ की क्षमताओं को कई तरीक़े से बढ़ा सकते हैं।
वह बताते हैं, “कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जो कुछ ही हफ़्तों में तनाव को कम करती हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने से डिमेंशिया जैसी बीमारियों को टाला जा सकता है और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक सदमे से मस्तिष्क को पहुंचे नुक़सान को कम किया जा सकता है।”
न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है?
– न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग़ की उस क्षमता को कहा जाता है, जिसमें वह बाहर से आने वाली सूचनाओं के आधार पर ख़ुद में बदलाव लाता है।
लखनऊ में मनोवैज्ञानिक राजेश पांडे ने बीबीसी हिंदी के लिए आदर्श राठौर को बताया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी वास्तव में हमारे दिमाग़ में मौजूद न्यूरॉन, जिन्हें नर्व सेल भी कहा जाता है, उनमें बनने और बदलने वाले कनेक्शन को कहा जाता है।
वह कहते हैं, “हमारा मस्तिष्क एक न्यूरल वायरिंग सिस्टम है. दिमाग़ में अरबों न्यूरॉन होते हैं. हमारे सेंसरी ऑर्गन (इंद्रियां) जैसे आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा बाहरी सूचनाओं को दिमाग़ तक ले जाते हैं. ये सूचनाएं न्यूरॉन के बीच कनेक्शन बनने से स्टोर होती हैं.”
“जब हम पैदा होते हैं तो इन न्यूरॉन में बहुत कम कनेक्शन होते हैं. रिफ़्लेक्स वाले कनेक्शन पहले से होते हैं, जैसे कोई बच्चा गर्म चीज़ के संपर्क में आने पर हाथ पीछे कर लेगा. लेकिन सांप को वह मुंह में डाल लेगा क्योंकि उसके दिमाग़ में ऐसे कनेक्शन नहीं बने हैं कि सांप खतरनाक हो सकता है. फिर वह सीखता चला जाता है और न्यूरल कनेक्शन बनते चलते हैं.” राजेश पांडे बताते हैं कि नए अनुभवों पर ये कनेक्शन बदलते भी हैं. इसी पूरी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है. इंसान के सीखने, अनुभव बनाने और यादों को संजोने के पीछे यही प्रक्रिया होती है।
* माइंडफ़ुलनेस का सीधा मतलब है- अपने आसपास के माहौल, अपने विचारों और अपने सेंसरी अंगों (आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा) को लेकर सचेत रहना. यानी बिना ज़्यादा मनन किए इस पर ध्यान देना कि उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं।
मनोवैज्ञानिक राजेश पांडे बताते हैं, “आसान भाषा में समझें तो माइंडफ़ुलनेस का मतलब है- इस बारे में सचेत होना कि हमारे सेंसरी ऑर्गन के ज़रिये बाहर से क्या जानकारियां दिमाग़ में जा रही हैं और अंदर मौजूद जानकारियों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है.” मेडिटेशन का उदाहरण देते हुए वह कहते हैं, “आसान भाषा में कहें तो यह अपने सेंसरी ऑर्गन पर फ़ोकस करने की प्रक्रिया है. अपनी सांस पर ध्यान देना या यह महूसस करना कि मौसम गर्म है या ठंडा, क्या मैं ठीक से सुन पा रहा हूं, क्या आसपास कोई सुगंध है.” “इससे भी न्यूरल कनेक्शन बनते हैं. आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान दिन में 15 मिनट ही इन सेंसरी अंगों पर ध्यान केंद्रित करे तो उसका चलना-फिरना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, सब बदल जाएगा।”
-bbc द्वारा
![]()
Discover more from जन विचार
Subscribe to get the latest posts sent to your email.